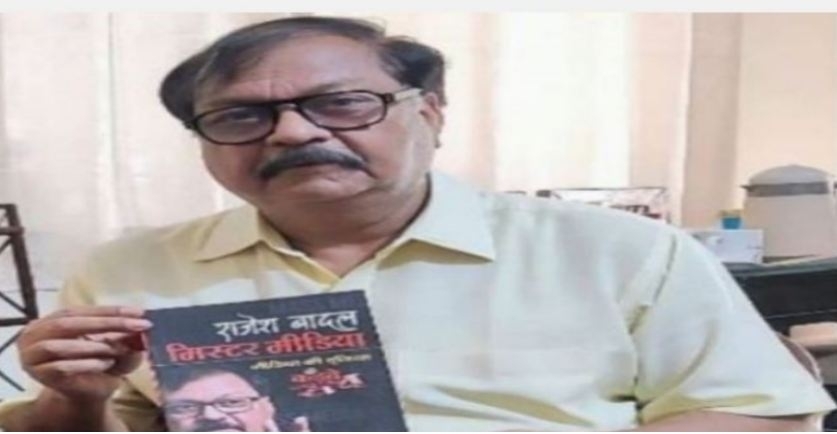राजेश बादल
इन दिनों भारतीय लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण दोराहे पर खड़ा है। सभी प्रदेशों के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएँ अथवा जैसा अभी चल रहा है ,वैसा ही चलने दिया जाए।इसके समर्थन में सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह दिया जा रहा है कि हिन्दुस्तान जैसे विराट विकासशील देश के लिए कम ख़र्च में इस लोकतान्त्रिक अनुष्ठान को संपन्न कराया जा सकता है। दो बार चुनाव कराने में अतिरिक्त व्यय को नियंत्रित किया जा सकता है और संबंधित प्रदेश की नौकरशाही को विकास कार्यों के लिए अधिक वक़्त मिल सकेगा।संभवतया कोविंद समिति ने इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी अनुशंषा की है।इसी भावना के तहत अब संसद भी विचार करेगी। कुछ राजनीतिक दलों ने इसी मक़सद से अपने निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के लिए सदन में मंगलवार को उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया था।
समूचे राष्ट्र में एक बार चुनाव के पक्ष में यह बात भी कही जा रही है कि आज़ादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू सरकार ने 1952 से 1962 तक एक साथ लोकसभा और सभी विधानसभाओं के निर्वाचन संपन्न कराए थे।इसलिए आज भी यह प्रासंगिक है।हालाँकि उस समय तो स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र की शुरुआत ही थी।सन 1951 में चुनाव क़ानून बना और चुनाव आयोग अस्तित्व में आया था।पूरे मुल्क़ में सारे चुनाव एक साथ कराने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था।इसलिए यह तर्क कि उन दिनों एक साथ जम्हूरियत का यज्ञ कराया जा सकता था तो आज भी हो सकता है - मुझे तनिक अटपटा लगता है।क्योंकि उन दिनों आज़ादी के आंदोलन से निकले तपे तपाए राजनेता थे और उनका नैतिक धरातल आज के सियासी माहौल से बहुत ऊपर था।हमारे तंत्र में धीरे धीरे जो राजनीतिक बीमारियाँ घर बनाती गईं,उनके कारण अनेक सियासी सिद्धांत,मूल्य,व्यवहार और आदर्श हाशिए पर चले गए।एक साथ चुनाव की यह स्वस्थ परंपरा भी विलुप्त होती गई।कराहता हुआ लोकतंत्र आगे बढ़ता रहा।संभव है कि आज के दौर में राजनीतिक नियंताओं के मन में फायदे की एक वजह यह भी हो कि अगर लोकसभा में किसी दल के पक्ष में मतदाता अपना वोट दे तो बहुत संभव है कि विधानसभा के लिए भी वह उसी पार्टी का चुनाव करे।इस तरह जो भी दल सत्ता में होगा,उसके दोनों हाथों में लड्डू होगा।उसे केंद्र में तो बहुमत मिलेगा ही और राज्यों में भी उसकी सरकारें बन जाएँ।इसके अलावा एक लाभ यह भी होगा कि केंद्र की छबि के आधार पर उसे प्रदेश में अपनी सरकार को बचाने का अवसर मिल जाए।वैसे यह नैतिक आधार पर उचित नहीं है क्योंकि उस दल की प्रदेश सरकार ने ख़राब प्रदर्शन किया हो तो अकर्मण्यता के बाद भी उसे पाँच साल का जनादेश मिल जाएगा।पर,नैतिक आधारों के लिए हमारे समाज में अब जगह कहाँ बची है ?
एक बार ग़ौर कीजिए कि उन्नीस सौ सत्तर तक देश में दलबदल की बुराई न्यून थी।आयाराम-गयाराम की कुप्रथा विकराल नहीं हुई थी।चुनाव में धन बल और बाहुबल का वैसा ज़ोर नहीं था,जैसा आज है।यह देखने में कभी नहीं आता था कि समूचे प्रचार अभियान में जो दल आमने सामने चुनाव लड़ते थे और वैचारिक आधार पर अलग अलग ध्रुवों पर खड़े हुए थे,वे निर्वाचन परिणाम आते ही सत्ता की मलाई चाटने के लिए एक होकर सरकार बना लेते हैं। हरियाणा इसका ताज़ा उदाहरण है।हम यह भी नहीं देखते कि चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरा दल या बहुमत प्राप्त गठबंधन सरकार बनाने की तैयारी कर रहा हो और देखते ही देखते उसके विधायक खरीद लिए जाएँ और वे पाला बदलकर पराजित पक्ष के साथ खड़े हो जाएँ।सरकार उसकी बने,जिसको जनादेश ही नहीं मिला था।इन दोनों स्थितियों में चुनाव लड़ने वाली दोनों पार्टियाँ जीत जाती हैं।मतदाता बेचारा हार जाता है।उसके वोट का मख़ौल उड़ता है।यह गणतंत्र का उपहास है।इसलिए इन राजनीतिक महामारियों के चलते एक देश - एक चुनाव की अच्छी मंशा के बाद भी उस पर संकट के काले बादल नहीं मँडराएँगे,इसकी कोई गारंटी नहीं है।
एक उदाहरण इसे समझने के लिए पर्याप्त होगा। मान लीजिए कि एक देश - एक चुनाव प्रणाली के तहत भारत में चुनाव हो गए और जीतने वाले दल या दलों ने केंद्र तथा राज्यों में अपनी अपनी सरकारें बना लीं तो वे निर्वाचित सत्ताएँ अपने पाँच साल पूरे करेंगीं ,यह कौन कह सकता है ? हालिया दशकों में भारतीय राजनीति की दशा और दिशा इस सन्दर्भ में आशा नहीं जगाती। सत्तारूढ़ पार्टियों के विधायकों का विपक्षी दलों ने शिकार किया और निर्वाचित सरकार गिरा दी गई। इसलिए चुनाव होने के बाद पाँच साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही धनबल से किसी प्रदेश की चलती हुई सरकार को अल्पमत में लाकर गिरा दिया जाए तो क्या यह लोकतंत्र की पराजय नहीं होगी ? दूसरी बात यह भी है कि यदि कोई राज्य सरकार पाँच साल पूरे नहीं कर पाती और विधायकों की ख़रीद -फ़रोख़्त से नई सरकार नहीं बन पाती तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। चुनाव के एक बरस बाद ही कोई सरकार अल्पमत में आ जाए तो क्या चार साल तक राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा,क्योंकि अगले चुनाव तो लोकसभा के साथ ही होने हैं। राष्ट्रपति शासन एक तरह से केंद्र सरकार की हुकूमत ही है।ऐसे में एक देश एक चुनाव की मंशा विकृत नहीं होगी ?यक़ीनन लोकतान्त्रिक भावना को भी ठेस पहुँचेगी क्योंकि प्रदेश का विकास निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के हाथों से ही हो सकता है। यही हमारा संविधान कहता है।जब निर्वाचित सरकार नहीं होगी तो ज़ाहिर है,प्रतिपक्ष भी नहीं होगा और असहमति के सुर भी ख़ामोश रहेंगे।उन्हें संरक्षण देने की बात तो बाद में आती है।अंतिम बात यह कि विधानसभा के निलंबित या भंग रहने की स्थिति में प्रदेश के स्थानीय मसलों का क्या होगा ? लोकसभा में तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विमर्श के लिए ही समय नहीं निकल पाता। साथ ही सांसद यह शिक़ायत करते हैं कि उनके संसदीय क्षेत्र के मामले सदन में पर्याप्त समय नहीं मिलने के कारण दम तोड़ देते हैं। फिर , एक विधायक के निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों का क्या होगा ? कुल मिलाकर यह कोई स्वस्थ परंपरा नहीं होगी।








198.jpg)
152.jpg)
24.jpg)
4.jpg)