वर्तमान सदी अपनी चौथाई उमर पूरी कर चुकी है। याने अब यह एक गबरू जवान के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है।पच्चीस बरस का हो रहा यह शताब्दी नौजवान वास्तव में मानसिक रूप से कितना परिपक्व हुआ है ? कह सकता हूँ कि उसकी देह या क़द काठी तो मज़बूत है लेकिन दिमाग़ी तौर पर यह सदी अभी बालिग़ नहीं दिखाई देती है।माँ बनने की क्षमता तो यह शताब्दी रखती है मगर संसार को संस्कारवान बना रही है,इसमें अभी संदेह है। इसका क्या अर्थ लगाया जाए ? हज़ार साल की लंबी ग़ुलामी के बाद हमारे सामने अपना लोकतंत्र तो आ गया लेकिन हमारे भीतर वह संकल्प बोध नहीं था ,जो किसी नवोदित आज़ाद मुल्क़ के भीतर होना चाहिए था। अँगरेज़ हमें देश थमाकर चले गए पर हम अपने पर राज करने की मौलिक शैली भूल चुके थे। सदियों तक परतंत्र रहते हुए भारत अपनी गणतांत्रिक जड़ों से अलग हो चुका था और बिना जड़ों के हम अपनी शासन शैली को ज़मीन में खोज रहे थे। यह ठीक है कि भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक पुरुषों ने आज़ाद होने से पहले ही इस कमज़ोरी को भाँप लिया था। इस कारण विश्व का श्रेष्ठ संविधान रचने की कवायद होती रही।
जब संविधान नामक नियामक संस्था हमारे बीच आई तो उन पूर्वजों या प्रतीक पुरुषों ने उसे अपनी गीता मानकर राष्ट्र में संविधान के नए बीजों से लोकतांत्रिक फसल लेने का प्रयास किया।यह प्रयोग कामयाब रहा।शायद इसलिए कि उस संविधान संस्था में हिंदुस्तान के बग़ीचे में मौजूद सारे फूल अपनी अपनी सुगंध के साथ उपस्थित थे। कोई एक फूल अपने आपको राजा फूल नहीं कह सकता था। सभी पुष्प इस गुलशन में अपनी अपनी महक के साथ उपस्थित थे। लेकिन बाद के दिनों में ऐसा लगने लगा कि शायद हमें स्वयं अपनी इस सुगंध से अरुचि हो गई है। उसका असर हमारी सियासत पर दिखाई दिया और धीरे धीरे भारतीय उपवन से जम्हूरियत की यह ख़ुशबू कम होती गई।पुराना सामंत बोध अपने नए विकृत स्वरूप में चुपचाप दाख़िल होता रहा। जाने माने संपादक और दार्शनिक चिंतक राजेंद्र माथुर ने पचपन साल पहले इसकी शानदार मीमांसा की थी। मैं यहाँ उनकी एक लंबी टिप्पणी पेश करना चाहूँगा। राजेंद्र माथुर राम नाम से प्रजातंत्र शीर्षक से 26 जनवरी 1969 को लिखे आलेख में कहते हैं ," जो हमने देखा है ,वही कर रहे हैं। शासक विदेशी थे ,इसलिए शासन प्रक्रिया भी हमारे लिए विदेशी हो गई।अब स्वराज है लेकिन हालत ज्यों की त्यों है। हम इस देश को ऐसे लूट रहे हैं ,जैसे यह देश हमारा नहीं ,बल्कि और किसी का हो। एक माने में भारत पर आज भी उन्ही शासकों का राज है। जनता और शासकों के बीच जो संगीतमय जुगलबंदी प्रजातंत्र में चलती है ,वह हमारे यहाँ ग़ायब है। मंत्री बनना या आई ए एस परीक्षा में पास होना हमारे यहाँ इतना महत्वपूर्ण क्यों है ? क्योंकि रेखा के उस पार जो विश्व है ,वह अलग है। वह विजेताओं का विश्व है।अँगरेज़ चले गए ,लेकिन रेखा के उस पार उनके साम्राज्य का प्रतिबिम्ब मौजूद है। जो आदमी नायब तहसीलदार बन जाता है ,वह भी रेखा के उस पार चला जाता है और विदेशी लुटेरा बन जाता है। महात्मा गांधी अगर राज्य का महत्व कम करना चाहते थे तो उसके पीछे अनेक प्रबल कारण थे। बड़ा कारण तो यह था कि हज़ार बरस से भूखे मरने वाले देश को पहले मौसंबी के रस की ज़रुरत थी ,दाल बाफलों की नहीं। गांधी अपने अंतर्मन में जानते होंगे कि भारत के बंदर ने कभी राज्य का उस्तरा पकड़ा ही नहीं है। शनैः शनैः इस देश की शासनेन्द्रिय का विकास होगा। सत्ता की सीमा और जनता की महिमा यह देश सीख सके ,इसके लिए कुछ वर्षों तक भारत को गांधी जैसे भक्त नेताओं की आवश्यकता थी ,जो कुर्सी - मुखी नहीं ,जन - मुखी होते। वे जनता को और शासकों को सिखाते कि अपने घर में नियम और संयम से कैसे रहा जाता है। लेकिन हुआ यह है कि राम नाम से प्रजातंत्र की ओर करंट इतनी तेज़ी से बढ़ा है कि शॉर्ट सर्किट हो गया है और सारे देश में अँधेरा घुप्प है। याने 15 अगस्त ,1947 के पहले भी अँधेरा था और अब भी है "।वे लिखते हैं ,एक हज़ार साल बाद लुटेरे गए हैं और हमारा घर हमें वापस मिला है। हम ,जो प्रेतों की तरह बल्लियों और खपरैलों पर बैठे थे,अब नीचे आ गए हैं। पर हम भूल गए हैं कि घर में कैसे रहा जाता है। वे कौन से संयम और स्नेह के तंतु हैं ,रिश्तों का वह कौन सा ताना बाना है ,जो परिवार को गरिमा और संतोष प्रदान करता है - हमें नहीं मालूम।
पचपन साल पहले लिखा गया यह आलेख आज भी प्रासंगिक इसलिए है कि आज सतहत्तर साल बाद भी हम दुविधा के इसी जाल में उलझे हुए हैं।हमने शासन करने के लिए एक प्रणाली तो बनाई ,लेकिन उसको मानने के लिए राष्ट्रीय चरित्र विकसित नहीं किया। आज़ादी के समय भले ही 18 फ़ीसदी साक्षरता रही हो ,पर उस समय के भारत में मानवीय और नैतिक मूल्यों का एक विराट भण्डार उपस्थित था। आज हम 75 प्रतिशत आधुनिकता के साथ उपस्थित हैं लेकिन राष्ट्रबोध नदारद है। यह एक निराशाजनक तस्वीर है। असल में ऐसी स्थिति तब बनती है ,जब मुल्क़ सियासी ढाँचे में ढलता तो है ,पर उसमें ज़िम्मेदारी और सरोकारों वाला नेतृत्व नहीं होता । एक ऐसा प्रेरक नेतृत्व ,जो हमारे समाज के सामने मुँह बाए खड़ी मुश्किलों को पार करने की हिम्मत और हौसला दे। यह काम खंड खंड समाज नहीं करता ,बल्कि एकजुट देश ही करता है। याद करिए कि जवाहर लाल नेहरू के ज़माने में भारतीय अगुआई भी दो हिस्सों में विभाजित थी। एक तरफ ओजस्वी,आज़ादी के आंदोलन से निकले तपे तपाए,विराट दृष्टिकोण वाले नेता थे तो दूसरी ओर संकीर्ण,अनुदार , कट्टर और छुटभैये नेताओं का बड़ा झुण्ड था। आसमान में सिर ले जाते नेहरू और ज़मीन पर रेंगने वाले कीट पतंगों के बीच कोई मंझली दुनिया नहीं थी। इसलिए अब न नेहरू का का रूमानी आदर्शवाद है ,न मज़बूत और स्वस्थ्य वातावरण है ,जो इस विशाल राष्ट्र की पतवार थामने का काम करे। अब केवल आत्मकेंद्रित सामंती और अराजक सोच है। बकौल साहिर लुधियानवी -
आओ ! कि आज ग़ौर करें इस सवाल पर ,देखे थे हमने जो ,वो हसीं ख़्वाब क्या हुए /
दौलत बढ़ी तो मुल्क़ में इफ़लास क्यों बढ़ा ,ख़ुशहालिए अवाम के असबाब क्या हुए /
मज़हब का रोग आज भी क्यों ला इलाज़ है ,वह नुस्ख़ा -हाय -नादिरो नायाब क्या हुए /










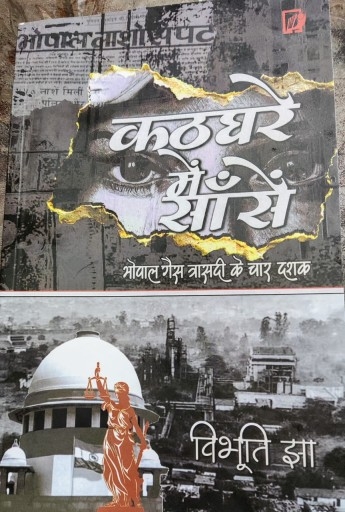
590.jpg)
476.jpg)
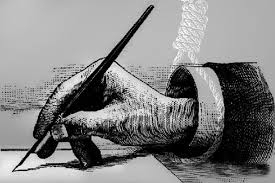
152.jpg)
198.jpg)
24.jpg)
4.jpg)




